मुक्तिबोध:प्रतिदिन (भाग-23)
पीले पत्तों के जग में
मेरे जीवन की फिलॉसफी उस सुख को स्थान नहीं था।
विष में थी पहिचान पुरानी मधु में तू अनजान नहीं था।
पतझर की कोकिल नीरव थी अंधकार में बंधन पाये,
पीले पत्तों के इस जग में जब झंझा से तुम बन आये।
जब तुझको समझा न सकी थी मेरे अंतस की ये आहें,
आँखों ने तब प्यार सम्हाला दे दुख को कितनी ही राहें।
करूणा की जीवन-झोली में मैंने किस सुख के कण पाये?
पीले पत्तों के इस जग में जब झंझा-से तुम बन आये।
(रचनाकाल 3 फरवरी, 1936। उज्जैन। रचनावली खंड 1 में संकलित)
मरण-रमणी
(मैने मरण को एक विलासिनी सुन्दरी माना है। और वह एक ऐसी सुन्दरी है जो कठोर नहीं है किन्तु हमारे अरमान पूर्ण करना ही मानों उसने धैर्य बना रखा है। पर एक शर्त पर, जो उससे विलास करने को राजी हो। मैंने उसे 'प्रेयसी', 'ममता-परी', 'सखी', 'आली', इत्यादि शब्दों से संबोधित किया है क्योंकि वह वैसी है भी। मरण -सुन्दरी हमें आकर्षण द्वारा खींचकर ले जाएगी, न कि यमदूतों के समान। वह हमें अपने अंचल से बाँधकर ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? जहाँ हमारे अरमान पूरे होंगे। ऐसा मेरा विशवास है?)
दीप बुझकर धूम्र छोड़ें, तारिकाएँ हट चलें सब!
आज शीतल ऊष्ण होंगे, ऊष्ण शीतल बन चलें सब!!
अवसाद यह उन्माद होकर गाढ़ तुझको चूम लेगा!!
मरण के उन्माद में सखी, आज कण-कण जल चलें सब।
प्यार-शैय्या पर पड़ा मै आज तेरी कर प्रतीक्षा,
ध्वांत है, घर शून्य है, उर शून्य तेरी ही समीक्षा!
मैं प्यार कर लूँ आज अंतिम, आज जग से जी लगा लूँ!
क्यों न उर से मैं लगा लूँ आज उनकी मृत्यु-दीक्षा।
( रचनाकाल 27 फरवरी 1936। उज्जैन। रचनावली खंड 1 में संकलित)
जीवन-यात्रा
मेरे जीवन का विराम!
नित चलता ही रहता है मेरा मनोधाम
गति में ही उसकी संसृति है
नित नव जीवन में उन्नति है
नित नव अनुभव है अविश्राम
मन सदा तृषित, सन्तत सकाम
मेरे जीवन का विराम।
कुछ महासागरों के आगे
था शान्त शून्य में द्वीप एक
भारान्वित हैं सौरभ अनेक!
जिसके सूनेपन में अकूल
फैले हैं खिलकर मृदुल फूल
जिसकी सूनी सांसों में बहती
रहती मंजुल गीत-धार
होकर अपने में ही अपार
जिसके मृदु तारों पर कंपकर
कंपन बन जाता स्वर-वितान
खुलकर खिलता उन्मुक्त भान।
कुछ महासागरों के आगे
उस मौन द्वीप में मधुर शान्त
चलने को पागल हो नितान्त
कुछ निकले नौकाएँ लेकर
वे भोले थे नारी औ नर
उत्ताल तरंगों से अड़कर
निर्बल से सबल हुए अन्तर
कुछ डूबे लहरों से लड़कर
वे रुके नहीं पर जीवन-भर
जो भोले थे नारी औ' नर।
औ' महासागरों की वे लहरें
भी भूखी थी प्रलयंकर
पर पहुँच गये सपने लेकर
सपनों के स्वामी नर अनेक
कुछ महासागरों के आगे
था शान्त शून्य में द्वीप एक!
(संभावित रचनाकाल 1937। इंदौर। आरती, जनवरी 1938 में प्रकाशित। रचनावली खंड 1 में संकलित)
दुख-सुख
दुख में ही सुख कर लो यारों,
दिल में पत्थर भर लो यारों।
जलती रहे चिता सुने में
हम उसको समझेंगे होली
जो हमको कमज़ोर बनाये
ऐसे सुख को मारो गोली
आँखों से चुपचाप सरकने
वाले आँसू पत्थर के हैं,
हम मजबूत, हमीं ने इनसे
सुख की सोना-चाँदी तौली।
काली घटा क्षितिज की देहली
चूम चली छाया आती है
बंजर पड़ी हुई धरती भी
हरियाली में मुसकाती है
दुख के धूएँ से काला पड़
गया बदन जिनका कुम्हलाया
उनकी सहज हास-रेखा भी
अति विद्रूप हुई जाती है।
कौंध रहा है बिजली बनकर,
वह विद्रूप हास इस दिल में
जैसे नाच रही हो साक़ी
एकाकी, सूनी महफिल में,
जैसे जड़ निर्जीव कब्र की
अभेद्य निद्रा भंग हुई हो
हिल उठी है बुनियादें
भूचालों की गहरी हलचल में।
(संभावित रचनाकाल 1937। इन्दौर। रचनावली खंड 1 में संकलित)
आत्मा के मित्र मेरे
मित्र मेरे,
आत्मा के एक!
एकाकीपने के अन्यतम प्रतिरूप।
जिससे अधिक एकाकी हृदय।
कमजोरियों के एकमेव दुलार
भिन्नता में विकस ले, वह तुम अभिन्न विचार
बुद्धि की मेरी शलाका के अरूणतम नग्न जलते तेज
कर्म के चिर-वेग में उर-वेग के उन्मेष।
वह हमारा मित्र है
माता-पिता-पत्नी-सुह्रद पीछे रहे हैं छूट
उन सबके अकेले अग्र में जो चल रहा है
ज्वलत तारक- सा,
वही तो आत्मा का मित्र है।
मेरे ह्रदय का चित्र है।
(संभावित रचनाकाल 1940-42। रचनावली खंड 1 में संकलित )
मृत्यु और कवि
क्षणभंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर,
दो सौ वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर?
इसी अमर धारा के आगे बहने के हित यह सब नश्वर,
सृजनशील जीवन के स्वर में गाओ मरण-गीत तुम सुन्दर।
तुम कवि हो, ये फैल चले मृदु गीत निबल मानव के घर-घर
ज्योतित हों मुख नव आशा से, जीवन की गति, जीवन का स्वर।
(संभावित रचनाकाल 1940- 1942। रचनावली खंड 1 में संकलित)
पूँजीवादी समाज के प्रति
इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि
इतना ज्ञान, संस्कृति और अन्त शुद्धि
इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति
यह सौन्दर्य, वह वैचित्र्य, ईश्वर-भक्ति,
इतना काव्य, इतने शब्द इतने छन्द-
जितना ढोंग, जितना भोग है निबंध
इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुन्दर जाल-
केवल एक जलता सत्य देने टाल
छोड़ो हाय, केवल घृणा औ' दुर्गन्ध
तेरी रेशमी वह शब्द-संस्कृति अन्ध
देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध
तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध
तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र
तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र
तेरे ह्रास में भी रोग कृमि है उग्र
तेरा नाश तुझ पर क्रूद्ध, तुझ पर व्यग्र।
( संभावित रचनाकाल 1940-42, रचनावली खंड 1 में प्रकाशित )
जीवन जिसने भी देखा है
जीवन जिसने भी देखा है
क्या पाया है, क्या लेखा है ?
क्या अपने में तृप्त हो चला ?
क्या संघर्षण-कोलाहल के
जीवन में वह शक्ति खो चला ?
जीवन की प्रत्येक परिस्थिति
धूप-छाँह सी, स्वर्ग -नरक सी,
जिसके लिए बनी है सुन्दर
काव्य-कथा -सी, एक व्यथा-सी
वह निरपेक्षित कलाकार-सा,
सब पर अंकन करता चलता।
अपने ही गुण-दोषों पर हो
मुग्ध, सदा जो बढ़ता चलता।
उसके उर की आग न ऐसी
जो बुझ सके स्निग्ध-वक्षों पर!
वह है ऐसी प्यास अनोखी
छोड़ चली जाती अपना घर!!
(विश्ववाणी अगस्त 1941 में प्रकाशित, रचनावली द्वितीय संस्करण में प्रकाशित )
जन-जन का चेहरा एक
चाहे जिस देश, प्रान्त, पुर का हो
जन-जन का चेहरा एक!
एशिया की, यूरोप की, अमरीका की
गलियों की धूप एक।
कष्ट -दुख सन्ताप की,
चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियाँ का रूप एक!
जोश में यों ताक़त से बन्धी हुई
मुट्ठियों का एक लक्ष्य!
पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर
है जनता का दल एक, एक पक्ष।
जलता हुआ लाल कि भयानक सितारा एक,
उद्दीपित उसका विकराल-सा इशारा एक,
गंगा में 'इरावती में, मिनाम में
अपार अकुलाती हुई,
नील नदी, आमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई,
बहती-बहाती हुई जिन्दगी की धारा एक,
प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक।
पृथ्वी का प्रसार
अपनी सेनाओं से किये हुए गिरफ्तार,
गहरी काली छायाएँ पसारकर,
खड़े हुए शत्रु का काले-से पहाड़ पर
काला-काला दुर्ग एक,
जन-शोषक शत्रु एक।
आशामयी लाल-लाल किरणों से अन्धकार
चीरता-सा मित्र का स्वर्ग एक,
जन-जन का मित्र एक।
विराट प्रकाश एक, क्रान्ति की ज्वाला एक,
धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक,
लाख-लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक,
हिये में हिम्मत का सितारा एक।
चाहे जिस देश, प्रान्त, पुर का हो
जन-जन का चेहरा एक
(संभावित रचनाकाल 1944-48। रचनावली खंड 1 में संकलित)
ओ , विराट स्वप्नों
ओ, विराट स्वप्नों, जागो
चाँदनी सरोवर-सी अपनी
आलोकभरी गहरी-गहरी आँखें खोलो!
रे, आज तुम्हारी प्राण-शक्ति की आवश्यकता,
आज तुम्हारी गान-शक्ति की आवश्यकता!
बन्द, अधखुले वातायन को,
अन्ध, धूम -विद्रूप सदन को
खंडहर की सूखी-सी तीखी
वायुभरे सूने आँगन को
आज तुम्हारी आँखों की उल्लास-रश्मि-सी,
स्नेह-चाँदनी के प्रवाह की आवश्यकता।
(संभावित रचनाकाल 1944-48। रचनावली खंड 1 में संकलित)
गुलामी की जंजीरें टूट जायेंगी
गुलामी की जंजीरें टूट सब जायेंगी,
उनको तोड़ देगा मेरा कसा हुआ बाहुदंड
भरे हुए वक्ष पर
उभरे हुए घावों की ये लाल-लाल लकीरें,
अनुभव के सहारे
मुझमें भर देंगी नये (खौलते-से) खून की
खिलखिलाती हुई सी बेचैन जवानियाँ।
मंजिल के लक्ष्य के लिए अकुलाती-सी
मीठी-मीठी सुलगती आग वह
जागेगी आँखों में सुबह का नूर बन।
गुलामी की जंजीरें जल्दी ही सब टूट जायेंगी
उनको तोड़ फेंक देगा
शक्तिशाली मेरा नया बाहुदंड।
पंक्षी के मानिंद हम नहीं उड़ जायेंगे
इन गलियों में चूहे-से नहीं ही सड़ेंगे हम
बनने के लिए हम इन्सान
कहाये हैं आदमी
मानव के लिए हम
हमारे लिए भी हम
गलियों में रहेंगे और गलियों में खायेंगे
गलियों में रहने वाले लोगों के लिए हम लड़ेंगे।
( अपूर्ण। संभावित रचनाकाल 1945-46। रचनावली खंड 1 में संकलित )
आधुनिक हिन्दी साहित्य और नवयुग की समस्याएँ
जब यह हम मान चुके कि हमारे राजनैतिक और सामाजिक अंगों का बहिष्कार करना, अपने हाथ और पैर को तोड़ देना है, तो हमें यह मान लेने में देरी नहीं करनी चाहिए कि व्यक्तिगत, या समूहगत भावनाओं से उठकर एक राष्ट्रात्मा भी होती है, जिसका शक्तिमान होना हमारी जीवनधारा के लिए निहायत जरूरी है। हम तब तक पूरी तरह से उन्नत नहीं हैं, जब तक की दूसरे आदमी हमारे समान ही उन्नत न हो जायें। दूसरों में बँट जाने वाला मैक्सिम गोर्की का कलाकार, आत्मा, इसी बात को समझकर, रशिया के एक कोने से लगाकर तो दूसरे कोने तक भटकता था।
इस समय युग में निश्चित परिवर्तन है। 'जीवन-धाराÓ अब आगे बढऩा चाहती है। पहले जब युग परिवर्तन हुआ, तब हम उपनिषत्काल के हिन्दुस्तान और मंसूर और जलालुद्दीन रूमी के मध्य एशिया में गये थे लेकिन आज हमारी दृष्टि भविष्य के सितारे पर है। भविष्य के हिन्दुस्तान पर है। और अगर आज हमारी और कला की धारा राष्ट्रात्मा से अलग होकर अपना मार्ग खोजती है, तो उसका रेगिस्तान में गुम हो जाना अपरिहार्य है।
(कर्मवीर, खंडवा। 4. मई 1940। रचनावली द्वितीय संस्करण में संकलित)
मेरे जीवन की फिलॉसफी उस सुख को स्थान नहीं था।
विष में थी पहिचान पुरानी मधु में तू अनजान नहीं था।
पतझर की कोकिल नीरव थी अंधकार में बंधन पाये,
पीले पत्तों के इस जग में जब झंझा से तुम बन आये।
जब तुझको समझा न सकी थी मेरे अंतस की ये आहें,
आँखों ने तब प्यार सम्हाला दे दुख को कितनी ही राहें।
करूणा की जीवन-झोली में मैंने किस सुख के कण पाये?
पीले पत्तों के इस जग में जब झंझा-से तुम बन आये।
(रचनाकाल 3 फरवरी, 1936। उज्जैन। रचनावली खंड 1 में संकलित)
मरण-रमणी
(मैने मरण को एक विलासिनी सुन्दरी माना है। और वह एक ऐसी सुन्दरी है जो कठोर नहीं है किन्तु हमारे अरमान पूर्ण करना ही मानों उसने धैर्य बना रखा है। पर एक शर्त पर, जो उससे विलास करने को राजी हो। मैंने उसे 'प्रेयसी', 'ममता-परी', 'सखी', 'आली', इत्यादि शब्दों से संबोधित किया है क्योंकि वह वैसी है भी। मरण -सुन्दरी हमें आकर्षण द्वारा खींचकर ले जाएगी, न कि यमदूतों के समान। वह हमें अपने अंचल से बाँधकर ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? जहाँ हमारे अरमान पूरे होंगे। ऐसा मेरा विशवास है?)
दीप बुझकर धूम्र छोड़ें, तारिकाएँ हट चलें सब!
आज शीतल ऊष्ण होंगे, ऊष्ण शीतल बन चलें सब!!
अवसाद यह उन्माद होकर गाढ़ तुझको चूम लेगा!!
मरण के उन्माद में सखी, आज कण-कण जल चलें सब।
प्यार-शैय्या पर पड़ा मै आज तेरी कर प्रतीक्षा,
ध्वांत है, घर शून्य है, उर शून्य तेरी ही समीक्षा!
मैं प्यार कर लूँ आज अंतिम, आज जग से जी लगा लूँ!
क्यों न उर से मैं लगा लूँ आज उनकी मृत्यु-दीक्षा।
( रचनाकाल 27 फरवरी 1936। उज्जैन। रचनावली खंड 1 में संकलित)
जीवन-यात्रा
मेरे जीवन का विराम!
नित चलता ही रहता है मेरा मनोधाम
गति में ही उसकी संसृति है
नित नव जीवन में उन्नति है
नित नव अनुभव है अविश्राम
मन सदा तृषित, सन्तत सकाम
मेरे जीवन का विराम।
कुछ महासागरों के आगे
था शान्त शून्य में द्वीप एक
भारान्वित हैं सौरभ अनेक!
जिसके सूनेपन में अकूल
फैले हैं खिलकर मृदुल फूल
जिसकी सूनी सांसों में बहती
रहती मंजुल गीत-धार
होकर अपने में ही अपार
जिसके मृदु तारों पर कंपकर
कंपन बन जाता स्वर-वितान
खुलकर खिलता उन्मुक्त भान।
कुछ महासागरों के आगे
उस मौन द्वीप में मधुर शान्त
चलने को पागल हो नितान्त
कुछ निकले नौकाएँ लेकर
वे भोले थे नारी औ नर
उत्ताल तरंगों से अड़कर
निर्बल से सबल हुए अन्तर
कुछ डूबे लहरों से लड़कर
वे रुके नहीं पर जीवन-भर
जो भोले थे नारी औ' नर।
औ' महासागरों की वे लहरें
भी भूखी थी प्रलयंकर
पर पहुँच गये सपने लेकर
सपनों के स्वामी नर अनेक
कुछ महासागरों के आगे
था शान्त शून्य में द्वीप एक!
(संभावित रचनाकाल 1937। इंदौर। आरती, जनवरी 1938 में प्रकाशित। रचनावली खंड 1 में संकलित)
दुख-सुख
दुख में ही सुख कर लो यारों,
दिल में पत्थर भर लो यारों।
जलती रहे चिता सुने में
हम उसको समझेंगे होली
जो हमको कमज़ोर बनाये
ऐसे सुख को मारो गोली
आँखों से चुपचाप सरकने
वाले आँसू पत्थर के हैं,
हम मजबूत, हमीं ने इनसे
सुख की सोना-चाँदी तौली।
काली घटा क्षितिज की देहली
चूम चली छाया आती है
बंजर पड़ी हुई धरती भी
हरियाली में मुसकाती है
दुख के धूएँ से काला पड़
गया बदन जिनका कुम्हलाया
उनकी सहज हास-रेखा भी
अति विद्रूप हुई जाती है।
कौंध रहा है बिजली बनकर,
वह विद्रूप हास इस दिल में
जैसे नाच रही हो साक़ी
एकाकी, सूनी महफिल में,
जैसे जड़ निर्जीव कब्र की
अभेद्य निद्रा भंग हुई हो
हिल उठी है बुनियादें
भूचालों की गहरी हलचल में।
(संभावित रचनाकाल 1937। इन्दौर। रचनावली खंड 1 में संकलित)
आत्मा के मित्र मेरे
मित्र मेरे,
आत्मा के एक!
एकाकीपने के अन्यतम प्रतिरूप।
जिससे अधिक एकाकी हृदय।
कमजोरियों के एकमेव दुलार
भिन्नता में विकस ले, वह तुम अभिन्न विचार
बुद्धि की मेरी शलाका के अरूणतम नग्न जलते तेज
कर्म के चिर-वेग में उर-वेग के उन्मेष।
वह हमारा मित्र है
माता-पिता-पत्नी-सुह्रद पीछे रहे हैं छूट
उन सबके अकेले अग्र में जो चल रहा है
ज्वलत तारक- सा,
वही तो आत्मा का मित्र है।
मेरे ह्रदय का चित्र है।
(संभावित रचनाकाल 1940-42। रचनावली खंड 1 में संकलित )
मृत्यु और कवि
क्षणभंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर,
दो सौ वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर?
इसी अमर धारा के आगे बहने के हित यह सब नश्वर,
सृजनशील जीवन के स्वर में गाओ मरण-गीत तुम सुन्दर।
तुम कवि हो, ये फैल चले मृदु गीत निबल मानव के घर-घर
ज्योतित हों मुख नव आशा से, जीवन की गति, जीवन का स्वर।
(संभावित रचनाकाल 1940- 1942। रचनावली खंड 1 में संकलित)
पूँजीवादी समाज के प्रति
इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि
इतना ज्ञान, संस्कृति और अन्त शुद्धि
इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति
यह सौन्दर्य, वह वैचित्र्य, ईश्वर-भक्ति,
इतना काव्य, इतने शब्द इतने छन्द-
जितना ढोंग, जितना भोग है निबंध
इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुन्दर जाल-
केवल एक जलता सत्य देने टाल
छोड़ो हाय, केवल घृणा औ' दुर्गन्ध
तेरी रेशमी वह शब्द-संस्कृति अन्ध
देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध
तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध
तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र
तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र
तेरे ह्रास में भी रोग कृमि है उग्र
तेरा नाश तुझ पर क्रूद्ध, तुझ पर व्यग्र।
( संभावित रचनाकाल 1940-42, रचनावली खंड 1 में प्रकाशित )
जीवन जिसने भी देखा है
जीवन जिसने भी देखा है
क्या पाया है, क्या लेखा है ?
क्या अपने में तृप्त हो चला ?
क्या संघर्षण-कोलाहल के
जीवन में वह शक्ति खो चला ?
जीवन की प्रत्येक परिस्थिति
धूप-छाँह सी, स्वर्ग -नरक सी,
जिसके लिए बनी है सुन्दर
काव्य-कथा -सी, एक व्यथा-सी
वह निरपेक्षित कलाकार-सा,
सब पर अंकन करता चलता।
अपने ही गुण-दोषों पर हो
मुग्ध, सदा जो बढ़ता चलता।
उसके उर की आग न ऐसी
जो बुझ सके स्निग्ध-वक्षों पर!
वह है ऐसी प्यास अनोखी
छोड़ चली जाती अपना घर!!
(विश्ववाणी अगस्त 1941 में प्रकाशित, रचनावली द्वितीय संस्करण में प्रकाशित )
जन-जन का चेहरा एक
चाहे जिस देश, प्रान्त, पुर का हो
जन-जन का चेहरा एक!
एशिया की, यूरोप की, अमरीका की
गलियों की धूप एक।
कष्ट -दुख सन्ताप की,
चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियाँ का रूप एक!
जोश में यों ताक़त से बन्धी हुई
मुट्ठियों का एक लक्ष्य!
पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर
है जनता का दल एक, एक पक्ष।
जलता हुआ लाल कि भयानक सितारा एक,
उद्दीपित उसका विकराल-सा इशारा एक,
गंगा में 'इरावती में, मिनाम में
अपार अकुलाती हुई,
नील नदी, आमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई,
बहती-बहाती हुई जिन्दगी की धारा एक,
प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक।
पृथ्वी का प्रसार
अपनी सेनाओं से किये हुए गिरफ्तार,
गहरी काली छायाएँ पसारकर,
खड़े हुए शत्रु का काले-से पहाड़ पर
काला-काला दुर्ग एक,
जन-शोषक शत्रु एक।
आशामयी लाल-लाल किरणों से अन्धकार
चीरता-सा मित्र का स्वर्ग एक,
जन-जन का मित्र एक।
विराट प्रकाश एक, क्रान्ति की ज्वाला एक,
धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक,
लाख-लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक,
हिये में हिम्मत का सितारा एक।
चाहे जिस देश, प्रान्त, पुर का हो
जन-जन का चेहरा एक
(संभावित रचनाकाल 1944-48। रचनावली खंड 1 में संकलित)
ओ , विराट स्वप्नों
ओ, विराट स्वप्नों, जागो
चाँदनी सरोवर-सी अपनी
आलोकभरी गहरी-गहरी आँखें खोलो!
रे, आज तुम्हारी प्राण-शक्ति की आवश्यकता,
आज तुम्हारी गान-शक्ति की आवश्यकता!
बन्द, अधखुले वातायन को,
अन्ध, धूम -विद्रूप सदन को
खंडहर की सूखी-सी तीखी
वायुभरे सूने आँगन को
आज तुम्हारी आँखों की उल्लास-रश्मि-सी,
स्नेह-चाँदनी के प्रवाह की आवश्यकता।
(संभावित रचनाकाल 1944-48। रचनावली खंड 1 में संकलित)
गुलामी की जंजीरें टूट जायेंगी
गुलामी की जंजीरें टूट सब जायेंगी,
उनको तोड़ देगा मेरा कसा हुआ बाहुदंड
भरे हुए वक्ष पर
उभरे हुए घावों की ये लाल-लाल लकीरें,
अनुभव के सहारे
मुझमें भर देंगी नये (खौलते-से) खून की
खिलखिलाती हुई सी बेचैन जवानियाँ।
मंजिल के लक्ष्य के लिए अकुलाती-सी
मीठी-मीठी सुलगती आग वह
जागेगी आँखों में सुबह का नूर बन।
गुलामी की जंजीरें जल्दी ही सब टूट जायेंगी
उनको तोड़ फेंक देगा
शक्तिशाली मेरा नया बाहुदंड।
पंक्षी के मानिंद हम नहीं उड़ जायेंगे
इन गलियों में चूहे-से नहीं ही सड़ेंगे हम
बनने के लिए हम इन्सान
कहाये हैं आदमी
मानव के लिए हम
हमारे लिए भी हम
गलियों में रहेंगे और गलियों में खायेंगे
गलियों में रहने वाले लोगों के लिए हम लड़ेंगे।
( अपूर्ण। संभावित रचनाकाल 1945-46। रचनावली खंड 1 में संकलित )
आधुनिक हिन्दी साहित्य और नवयुग की समस्याएँ
जब यह हम मान चुके कि हमारे राजनैतिक और सामाजिक अंगों का बहिष्कार करना, अपने हाथ और पैर को तोड़ देना है, तो हमें यह मान लेने में देरी नहीं करनी चाहिए कि व्यक्तिगत, या समूहगत भावनाओं से उठकर एक राष्ट्रात्मा भी होती है, जिसका शक्तिमान होना हमारी जीवनधारा के लिए निहायत जरूरी है। हम तब तक पूरी तरह से उन्नत नहीं हैं, जब तक की दूसरे आदमी हमारे समान ही उन्नत न हो जायें। दूसरों में बँट जाने वाला मैक्सिम गोर्की का कलाकार, आत्मा, इसी बात को समझकर, रशिया के एक कोने से लगाकर तो दूसरे कोने तक भटकता था।
इस समय युग में निश्चित परिवर्तन है। 'जीवन-धाराÓ अब आगे बढऩा चाहती है। पहले जब युग परिवर्तन हुआ, तब हम उपनिषत्काल के हिन्दुस्तान और मंसूर और जलालुद्दीन रूमी के मध्य एशिया में गये थे लेकिन आज हमारी दृष्टि भविष्य के सितारे पर है। भविष्य के हिन्दुस्तान पर है। और अगर आज हमारी और कला की धारा राष्ट्रात्मा से अलग होकर अपना मार्ग खोजती है, तो उसका रेगिस्तान में गुम हो जाना अपरिहार्य है।
(कर्मवीर, खंडवा। 4. मई 1940। रचनावली द्वितीय संस्करण में संकलित)
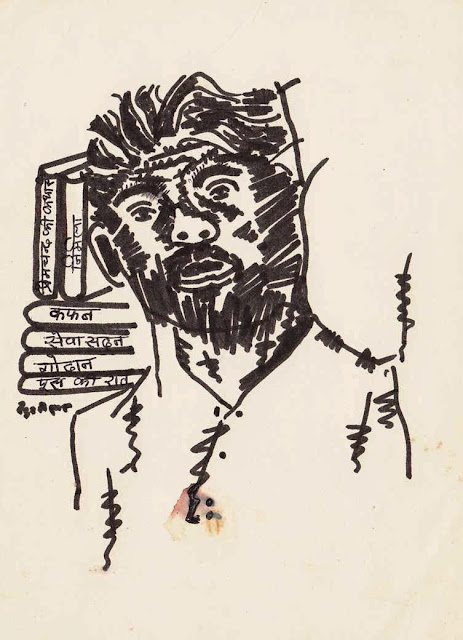


Comments
Post a Comment