मोहब्बत नहीं नफ़रत को ढोती राजनीति
- दिवाकर मुक्तिबोध
2019 का लोकसभा चुनाव अब अंतिम दौर में है। 19 मई को अंतिम चरण के मतदान के बाद 23 मई का इंतज़ार। इस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के इतिहास में व्यक्तिगत आक्षेपों व अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कुख्यात यह चुनाव और भी कई मायनों में यादरखा जाएगा। नतीजों को लेकर भी और व्यक्तित्व की दृष्टि से भी। इस चुनाव में बहुचर्चित नाम- कन्हैया कुमार। जेएनयू दिल्ली छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष।
बेगूसराय से सीपीआई के युवा प्रत्याशी। अपने धारदार भाषणों व सत्ता विरोधी तेवरों से कन्हैया ने देश के पढ़े -लिखे मतदाताओं का ध्यान ठीक उसी तरहसे आकर्षित किया जैसा वर्ष 2012-13 में अरविंद केजरीवाल ने किया था। अन्ना आंदोलन से उपजे केजरीवाल दिल्ली ही नहीं , दिल्ली से बाहर भी राष्ट्रीयराजनीति में एक संभावना बनकर उभरे थे। बेहतर कल की संभावना।
इसे आधार दिया था दिल्ली प्रदेश के मतदाताओं ने जिन्होंने फ़रवरी 2015 में विधानसभा के दुबारा हुए चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ऐसा प्रचंड बहुमत दिया जो भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन गया। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। यह चुनाव इस मायने में भी अभूतपूर्व रहा कि 135 साल पुरानी कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला।कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास की यह पहली घटना थी जिसमें दिल्ली के मतदाओं ने उसे सिरे से ख़ारिज कर दिया। भाजपा के लिए भी यह गहरा धक्का था क्योंकि देश भर में चली मोदी -आँधी के चलते 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था और नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। मोदी -आँधी का वेग थमा नहीं था लेकिन इसके बावजूद भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके सिर्फ तीन विधायक चुनकर आए। यह आश्चर्यजनक हार थी।
एक नई नवेली पार्टी की तूफ़ानी जीत से देश भर में यह संदेश गया कि कांग्रेस व भाजपा का राष्ट्रीय विकल्प तैयार हो रहा है। राष्ट्रीय राजनीति मे इसेसुखद हवा का झोंका माना गया लेकिन बहुत जल्दी यह बात स्पष्ट हो गई कि मौजूदा भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय तमग़े के होते हुए भी किसी भी पार्टी केलिए समूचे राष्ट्र का चेहरा बनना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल जिस तरह गुज़रे हैं, उसे देखते हुए इस निष्कर्ष परपहुँचना कठिन नहीं है कि इस पार्टी का भी सफ़र क्षेत्रीयता से परे नहीं है । यानी यह कहा ज़ा सकता है कि है कि देश के नौजवानों ने व सर्वहारा वर्ग ने आमआदमी पार्टी को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में तैयार होते देखा था, उसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है।
लेकिन इसमें दो राय नहीं कि केजरीवाल एक संभावना बनकर उभरे थे। कन्हैया कुमार भी एक संभावना है । दोनों का क़द पार्टी से बडा है।देश का बौद्धिकवर्ग कन्हैया को ओजस्वी वक़्ता और स्पष्ट विचारों वाले युवा नेता के रूप में ज़्यादा जानता हैं । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके पीछे ज़रूर खड़ी है पर उम्मीदें कन्हैया से है पार्टी से नहीं जो बहुत तेजी से अपनी आभा व जनाधार खोते जा रही है। इसलिए सवाल है , समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले कन्हैया , जिग्नेश मेवाड़ी , हार्दिक पटेल ,अल्पेश ठाकोर, चन्द्रशेखर रावन जैसे अनेक प्रतिभाशाली युवा नेता जिस तीव्रता से देश-प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बना रहे है , क्या इससे इसके शुद्धीकरण की कुछ उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन इस पर विचार करते समय ध्यान में यह बात भी आती है कि इनके पूर्व भी अनेक नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया और वह भी तब जब राजनीति आज जैसी दूषित नहींथी, नैतिकता के कुछ रेशे व मूल्यों के चंद अक्स शेष थे इसलिए उसे पटरी पर लाने की उम्मीदें बाक़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उस दौर में ताज़ी हवा का जो झोंका आया वह थोड़ा बहुत असर ही डाल सका। राजनीति में गंदगी आती चली गई जिसकी धारा अविरल है। इस धारा का ही प्रताप है कि उसने स्थितियाँ बहुत बदल दी है। घृणा , नफ़रत और कदाचार ने राजनीति को एकदम निचले स्तर तक पहुँचा दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि 2014 के चुनाव मेंनेताओं के भाषणों व चुनाव प्रचार में भाषा का संयम कुछ हद तक बरक़रार था लेकिन इस बार के लोक सभा चुनाव में यह सिरे से ग़ायब हो गया। चुनावप्रचार में सारी मान-मर्यादाएं ताक पर रख में दी गई। कांग्रेसी वक्ताओं के चौकीदार चोर है या फेंकू नंबर एक जैसे जुमले ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही , प्रधानमंत्री जैसे अति महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की गरिमा भी खंडित कर दी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने पता नहीं क्यों अपने अध्यक्ष राहुल गांधी को यह समझाइश नहीं दी कि उन्हें अपने भाषणों में चौकीदार चोर जैसी निम्न स्तरीय जुमले का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मौक़ा कोई भी हो , कांग्रेस हमेशा अपने प्रतिपक्ष के सम्मान का ध्यान रखते आई है। मलाल इस बात का अधिक है कि स्वयं प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं रहे। बल्कि दो क़दम आगे रहे। उन्होंने नेहरू -गाँधी परिवार और ख़ासकर स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति जिस तरह अशोभनीय व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया वह न केवल दुखद है वरन यह भी इंगित करता है कि देश के लोगों ने कैसे व्यक्ति को देश की कमान सौंप रखी है।
नीतियों व मुद्दों पर बात करने के बजाए राष्ट्रवाद व शहीदों के नाम पर वोट माँगने वाला प्रधानमंत्री देश ने पहले कभी नहीं देखा। यों भी जाति व धर्म वोटों की राजनीति के सबसे बड़े हथियार रहे हैं और अब इसमें देश के लिएजान क़ुर्बान करने वाले शहीदों के नाम पर राष्ट्रवाद का तडका लगाने में नरेन्द्र मोदी व उनकी पार्टी भाजपा ने कोई गुरेज़ नहीं किया है। चुनावी राजनीति मेंऐसा पहली बार हुआ है जब सेना को भी इसमें घसीटने का प्रयत्न हुआ हो। यह बहुत ही ख़तरनाक प्रवृत्ति है जो तानाशाही की पीठ पर सवार रहती है।राजनीति को इससे बचने की ज़रूरत है। एक बहुलता वाले देश में जहाँ लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी होने के बावजूद राजनीति पतन के इस मोड़ पर पहुँच गईहो तो कन्हैया सरीखे आदर्शवादी व ज़मीन से जुड़े नए युवा नेता कितना कुछ कर पाएँगे, संदेह है। लेकिन ना उम्मीदौं के बीच एक लौ टिमटिमाती हुई ज़रूरदिखती है जो निपट अंधेरे को सर्वत्र उजाले से भर देती है।यह उम्मीद भले ही वह ख़ुशफ़हमी ही क्यों न हो, हम पाल ही सकते हैं।
दरअसल राजनीति के शुद्धीकरण के लिए राजनयिकों का मन व विचारों से शुद्ध होना जरूरी है। यह लगभग असंभव जैसा है। इस स्थिति में युवा पीढ़ी सेज़रूर उम्मीद की जा सकती जो जोश-खरोश के साथ कुछ बेहतर करने बेताब रहती है।ऐसे युवाओं का राजनीति में दखल जरूरी है । केवल एक कन्हैयाकुमार या हार्दिक पटेल या केजरीवाल से काम नहीं चल सकता। छात्र राजनीति से निकले ऐसे प्रखर व प्रतिभाशाली युवाओं की फ़ौज चाहिए जो राजनीति कोखाई में गिरने से पहले पीछे खींच के लाए। कन्हैया कुमार संसद में पहुँचे या न पहुँचे , हार्दिक पटेल या जवान तेज़ बहादुर यादव को भले ही चुनाव लड़ने सेरोका जाए , लेकिन उनकी आवाज़ में जब असंख्य आवाज़ें मिलेंगी, समझिए वह दिन सकारात्मक बदलाव की राजनीति का दिन होगा और लोकतंत्र का सबसे पवित्र दिन भी।
क्या यह मुमकिन है? शत-प्रतिशत न सही, राजनीति को कुछ हद तक सँवारा जा सकता है बशर्ते संवैधानिक संस्थाएँ अपने अधिकारों को पहिचाने व उनका युक्तिसंगत उपयोग करें। एक टी एन शेषन ने विशेष कुछ नहीं किया था । केवल अपने अधिकारों को जाना और तदनुसार कार्य करतेहुए चुनाव आयोग की चुनावों के दौरान सर्वोच्चता कायम की लेकिन वही चुनाव आयोग फिर जस का तस हो गया है , पराधीन और पक्षपाती। तो यह माननाहोगा कि राजनीति में सुधार की प्रक्रिया बहुत जटिल व दीर्घकालीन है। इसमें निरंतरता चाहिए, तात्कालिकता नहीं।

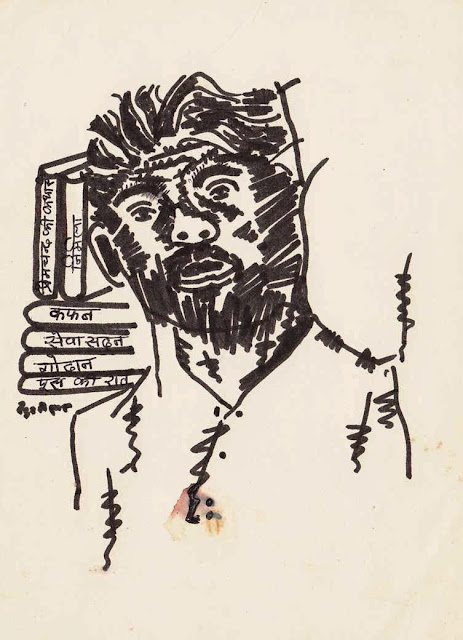


Comments
Post a Comment