कुछ यादें कुछ बातें - 19
-दिवाकर मुक्तिबोध
तो, 70 का वह दशक यानी वह दशक जब मैं नौजवान था और पत्रकारिता की एबीसीडी सीखने का प्रयत्न कर रहा था, बहुत मजेदार और जीवंत था। नौजवानी में वैसे भी मन उमंग और उत्साह से भरा रहता है तथा जिंदगी, तमाम कठिनाइयों, दुश्वारियों के बावजूद दिलकश लगती हैं। संघर्ष में आदमी टूटता नहीं था बल्कि तपता व मजबूत होता था। मेरी स्थिति भी ऐसी ही थी। घर में दिक्कतें थीं जो घर में ही महसूस होती थी, दफ्तर आते ही उड़नछू। सारे दर्द और चिंताएं भूलकर हम अपने काम में मशगूल हो जाते थे। काम का काम और साथ में हंसी ठट्टा भी। ऐसा लगता था जिंदगी कहीं हैं तो दफ्तर में ही है। मैंने कहा था न कि, मैं जिनसे बहुत प्रभावित था, वे थे राजनारायण, मेरे पहले गुरु। दूसरे अखबार के युवा प्रोपाइटर ललित सुरजन, तीसरे रम्मू भैय्या (रामनारायण श्रीवास्तव) श्रीवास्तव और चौथे सत्येन्द्र गुमाश्ता। इन महागुरुओं के बारे में थोड़ा सा बता दूं -: राजनारायणजी प्रांतीय खबरों के ओव्हर ऑल इंचार्ज, ललित सुरजनजी मालिक कम पत्रकार ज्यादा, पूरे अखबार के संयोजन व प्रबंधन की महती जिम्मेदारी। रम्मू श्रीवास्तव और सत्येन्द्र गुमाश्ता राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय तमाम किस्म की खबरों का संपादन व संयोजन विशेषत: प्रथम पृष्ठ के जिम्मेदार। ये चारों मेरे लिए आदर्श के प्रतिमान थे हालांकि सभी का स्वभाव अलग-अलग था पर काम के सभी पक्के। पेशेगत ईमानदारी के कायल। राजनारायणजी और रम्मू भैय्या अत्यधिक विनम्र और खुशमिजाज। ललित सुरजनजी और सत्येन्द्र गुमाश्ता तनिक गुस्सैल। किन्तु दिल के साफ। रम्मू भैय्याजी के बारे में मुझे पता था कि वे राजनांदगांव के थे। मेट्रिक के बाद घर से निकले व नागपुर चले गए। नागपुर में अखबार 'नया खूनÓ में कम्पोजिटर बन गए। नया खून प्रगतिशील विचारों का प्रसिद्ध अखबार था। इसी अखबार में वे दीक्षित हुए। वे धीरे-धीरे प्रगति की सीढिय़ां चढ़ते गए और जब रायपुर-राजनांदगांव लौटे तो उनकी ख्याति एक ऐसे पत्रकार के रुप में थी जिसकी कलम की धार बहुत तेज थी तथा उनके साप्ताहिक स्तंभ बहुत चाव से पढ़े जाते थे। श्यामवर्ण के रम्मू भैया 50 के आसपास थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान तैरा करती थी। होठों में सिगरेट दबाए रखते थे और धुएं के छल्ले बनाकर हवा में उड़ाना, उनका शगल था। वे इसमें मस्त रहते थे। सिगरेट कभी होठों से अलग नहीं होती थी। एक बुझी नहीं कि दूसरी तैयार। चेन स्मोकर थे।
60-70 के उस दौर में कस्बाईनुमा शहरों की जैसी जिंदगी होती है, वैसे ही रायपुर की थी। राजनीतिक रुप से गर्म एक ऐसा शहर जो अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य की राजनीति की दिशा तय करता था। श्यामाचरण शुक्ल इसी शहर के थे जो मध्यप्रदेश के तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रहे। विद्याचरण शुक्ल केंद्रीय मंत्री के रुप में बरसों राज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे। दरअसल वह दौर शुक्ल बंधुओं के प्रभामंडल का था। छत्तीसगढ़ की ही नहीं मध्यप्रदेश की राजनीति के वे शीषस्थ थे। विपक्ष टूटा व बिखरा हुआ था। विपक्ष के नाम पर राजनीति में कुछ हैसियत जनसंघ की थी। वामपंथी पार्टियां भी मौजूद थी लेकिन इसके बावजूद मध्यप्रदेश विशेषकर छत्तीसगढ़ में उनकी जड़ें नहीं के बराबर थी। इस तरह समूचा विपक्ष प्रभावहीन व शक्तिहीन था। पूरे राज्य में कांगे्रस का वर्चस्व था। देश में रायपुर की विशिष्ट पहचान थी। दरअसल वह मुख्यत: विद्याचरण शुक्ल की वजह से थी। राज्य के बाहर के लोग कहते थे - 'अरे रायपुर, विद्याचरण शुक्ल का रायपुरÓ शहर खुली हवा में सांस लेता था। धुआं उगलने वाले कारखाने नहीं थे अलबत्ता आसपास औद्योगिक बसाहट की नींव जरुर रखी जा रही थी। धीमी रफ्तार का अलसाया सा शहर लेकिन खुशमिजाज। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढिय़ों के आकर्षण का केंद्र था रायपुर जो गरीब आदिवासियों, हरिजनों व निम्न, मध्यम वर्गीय जनता को उस दौर की अपनी भव्यता, समृद्धता से आतंकित भी करता था क्योंकि उनके अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने गांव में ऐसी जिंदगी सुलभ नहीं थी। इसलिए उसे निहारने, रोजी-रोटी कमाने की गरज लिए ग्रामीणों का रेला, रायपुर आया ही करता था, अभी भी आता है। कोतवाली के पास गांधी मैदान में मजदूरों की बड़ी मंडी थी जो आज भी कायम है। दरअसल प्राय: हर बड़े शहर में एक ऐसा ठिकाना तो होता ही है जहां दीन-दरिद्र पर मेहनतकश मजदूर दिन की रोजी पक्के करने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होते है। जहां श्रम की खरीद-फरोख्त होती हैं। और सुबह घंटे-दो घंटों में लगभग आधी से अधिक भीड़ छंट जाती हैं पर जिन्हें काम नहीं मिलता, वे कोई तो आएगा की आस में लगभग आधा दिन मंडी में डटे रहते हंै और अंतत: निराश होकर खाली पेट और परिवार की चिंता लिए दिन डूबने तक शहर की गलियां व सड़कें नापने लगते हैं। एक नवंबर सन् 2000 में नया राज्य बनने के बाद यकीनन छत्तीसगढ़ में समृद्धता बढ़ी, बड़े-बड़े उद्योग धंधे खुले किन्तु कुटीर उद्योगों का सत्यानाश हुआ, खेती-किसानी, प्रकृति के मिजाज पर ही आश्रित रही, काम की तलाश में मजदूर पहले जैसे ही दूसरे राज्य की ओर पलायन करते रहे। यानी समृद्धता तो बढ़ी पर किसके लिए? मजदूर-मजदूर ही रहा। बाप मजदूर, बेटा मजदूर, बेटे का बेटा मजदूर। सस्ता श्रम, इतना सस्ता कि गाँव-देहातों के जमीनदारों के यहाँ, जागीरदारों के यहाँ, साहूकारों के यहाँ, सूदखोरों के यहां तो श्रमिक बंधक के रुप में जिंदगी बसर करते थे। उनका कोई निजी अस्तित्व नहीं था। बंधुआ श्रमिकों की जमात अभी भी लगभग वैसी ही है। पूरी जिंदगी के लिए गुलामी। अलिखित पट्टा। आर्य समाजी स्वामी अग्निवेश ने इन बंधुआ मजदूरों को पीढ़ी दर पीढ़ी की गुलामी से मुक्त करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया, बंधुआ श्रमिकों को शोषकों से मुक्त भी किया किन्तु क्या बंधुआ पद्धति खत्म हो गई? यह आज भी जारी हैं, शोषण के विभिन्न रुपों में, छत्तीसगढ़ में भी और छत्तीसगढ़ के बाहर भी।
अब चंद बातें अखबारों की। अविभाजित मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना समाचारपत्र दैनिक महाकोशल। बाद में नवभारत, देशबन्धु व युगधर्म। कुछ दर्जन साप्ताहिक अखबार भी। विशेषकर राजनांदगांव से सर्वाधिक। नया राज्य बनने के बाद दैनिक समाचार पत्रों की संख्या बढी व दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका व हरिभूमि ने पैर पसार लिए व प्रसार की दृष्टि से पुरानों को पीछे कर दिया। युगधर्म का प्रकाशन तो खैर वर्षों पूर्व बंद हो गया था। बीते बीस वर्षों में राज्य मेंं एक के बाद एक बहुत से इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल के ब्यूरो शुरू हो गए तथा कुछ प्रादेशिक भी। अब सोशल मीडिया पर न्यूज प्लेटफार्म, न्यूज पोर्टल की बाढ सी है। यानी समय के साथ मीडिया भी बेहद विस्तारित हुआ है। प्रिंट मीडिया में अखबारों के कामकाज का तौर तरीका बदला पर आधारभूत संरचना पूर्व जैसी ही है। रीजनल डेस्क सर्वाधिक प्रभावी पहले भी थी, अभी भी है। हमारे समय में और वर्तमान दौर में भी सबसे ज्यादा खबरें इसी डेस्क पर आती थी। सर्कुलेशन के दायरे में आने वाले शहरों के संवाददाता, गांव कस्बों के संवाददाताओं की खबरें बाई पोस्ट आती थी। 1000-500 की आबादी वाले गाँवें में भी अखबार पहुंचता था। ग्रामीण संवाददाता भले ही ज्यादा पढ़े-लिखे न हो, भले ही उनके जिम्मे अखबार का प्रसार बढ़ाने व विज्ञापन इक_ा करने का भी दायित्व क्यों न हो किन्तु खबरों के मामले में वे पक्के रहते थे। जागरुक थे। उनकी भाषा भले ही लचर हो पर वे घटना का ब्यौरा ठीक से रख पाते थे। हमारा काम था शब्दों के बीच पसरे हुए भावों को ठीक से समझना व उनका पुनरलेखन करना। इसलिए खबरों की जो फाइनल कापी बनती थी, वह सुघड़ रहती थी। वह संपादित होती थी, सरल भाषा व शैली में लिखी होती थी ताकि सामान्य पाठक भी उन्हें आसानी से समझ सकें। चूंकि खबरों की तादाद बहुत रहती थी, इसलिए इस डेस्क पर काम का बोझ ज्यादा रहता था। काम अधिक रहता था लिहाजा इसी डेस्क पर सहयोगियों की संख्या भी ज्यादा रहती थी। लेकिन अब, आज के दौर की पत्रकारिता में यह डेस्क महत्वपूर्ण होते हुए भी पूरी तरह उपेक्षित है। अब खबरों का पुर्नलेखन नहीं होता, खबरें डाक से नहीं, कम्प्यूटर पर आती हैं। लिहाजा वही उनकी कांट-छांट होती है। अच्छी, सरल और त्रुटिहीन भाषा अब प्राथमिकता में नहीं है। जैसा ग्रामीण या कस्बाई संवाददाता खबरें भेजता है, वे लगभग वैसी ही अखबारों में परोस दी जाती है। टूटी-फूटी भाषा,अनावश्यक विस्तार। कल और आज की क्षेत्रीय पत्रकारिता में यह बड़ा फर्क आया है। भाषा से ध्यान हट गया है, खबरों के संपादन के लिए बैठे पत्रकारों के लिए अब भाषा-ज्ञान जरुरी नहीं है। समझा जा सकता है कि जब डेस्क संपादकों की ही भाषा ठीक न हो तो वह खबरों का संपादन किस तरह करता होगा। एक और दिक्कत यह है कि अखबारों के संपादकों को भी इसकी परवाह नहीं रह गई है। जाहिर है अखबारों की भाषा, विशेषकर प्राविंशियल खबरों की भाषा पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है। इसका एक और दुष्परिणाम पत्रकारों का भाषा के मामले में दीक्षित न हो पाना है। वह इसलिए क्योंकि लिखने-पढऩे व समझने की संस्कृति लगभग खत्म होती जा रही है। दरअसल अब क्षेत्रीय अखबारों में आमतौर पर नियुक्ति के समय इंटरव्यू के दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि प्रार्थी की भाषा, उसका लेखन व सामान्य ज्ञान समृद्ध है अथवा नहीं। पहले अनुभव व माहौल से युवा पत्रकार सीखते चले जाते थे और अब शुरुआत से ही स्वयं को समर्थ मानने लगते हैं।
----------
(अगली कड़ी शनिवार 9 अक्टूबर को)
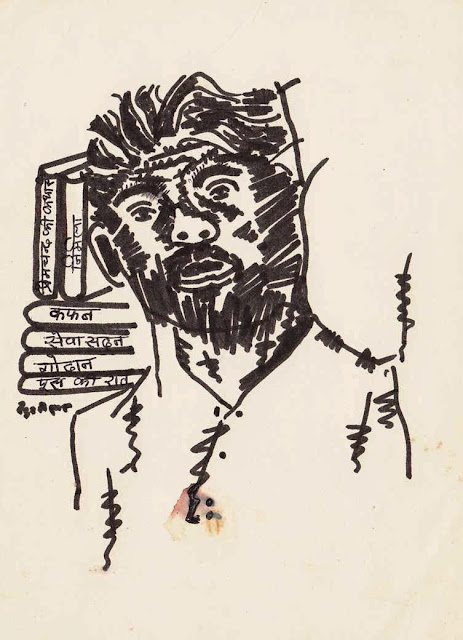


Comments
Post a Comment